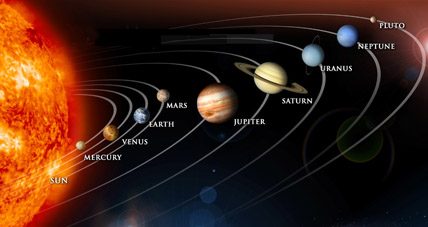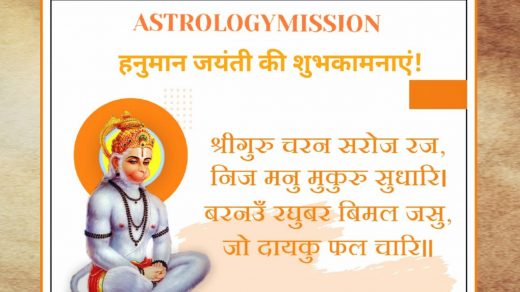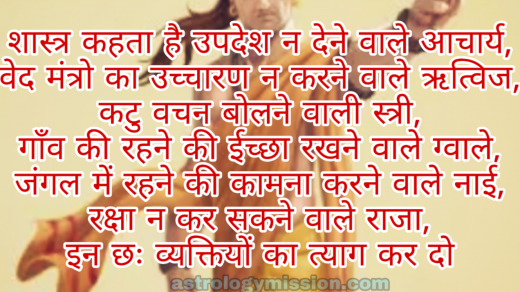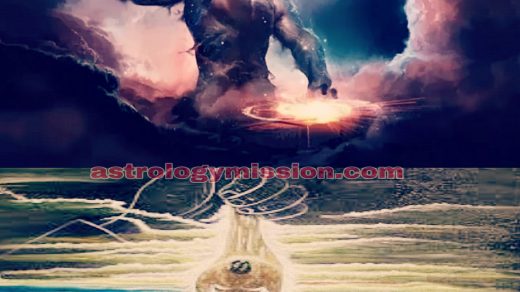![]()

“ योगाभ्यास से सर्व ऐश्वर्यो की सिद्धि “
*******************
योग :- महर्षि पतंजलि के अनुसार- ” योगश्चित वृत्तिनिरोधः “
अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोग ही योग है ।
योग के प्रमुख भेद और अवस्थाएं
~~~|||~~~~~|||~~~~~~~
प्रमुख चार भेद हैं:-
१- मन्त्र योग
२- लययोग
३- हठ योग
४- राजयोग
उपरोक्त चारो योगो की चार चार अवस्थाएं हैं
अ- आरम्भ
ब- घट
स- परिचय
द- निष्पत्ति
१- मंत्र योग :- जो मात्रा जप बारह सौ की संख्या में करता है, वह क्रम से अणिमादि गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह अल्प बुद्धि, अधम श्रेणी के साधक करते हैं।
२- लय योग :- करोड़ों बार चित्त का लय होना अर्थात चलते बैठते सोते और भोजन करते समय निष्फल परमात्मा के ध्यान में नितांत मग्न हो जाना।
३- हठ योग :- यह अष्टांग योग है।
^^^^^^^^^^
१- यम
२- नियम
३- आसन
४-प्राणायाम
५- प्रत्याहार
६- धारणा
७- ध्यान
८- समाधि
1- यम;- लघु आहार ही मुख्य यम है। यह योग का प्रथम अंग माना गया है।यम के पाँच प्रकार है।
१-अहिंसा
२- सत्य
३- अस्तेय
४- ब्रह्मचर्य
५-अपरिग्रह
1- अहिंसा :- अहिंसा का साधारण अर्थ है हिंसा का करना, अर्थात शारीरक एवं मानसिक स्तर पर किसी को भी यातना न देना। प्राणी मात्र मे हिंसा न करना। मनुष्य समस्त जीव जन्तु मे प्यार सहानुभूति तथा समानता का व्यवहार करना, अहिंसा व्रत का पालन होता है।
2- सत्य :- सत्य का साधारण अर्थ है वासत्विकता मे जीवन यापन करना, मनोबल एवं आत्मशक्ति का विकास करने के लिए सत्य को अपनाना चाहिए।
3- अस्तेज :- इसका सामान्य अर्थ है चोरी न करना, जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं, उस पर अधिकार न करना, बिना इजाजत के किसी वस्तु को न उठाना, मानसिक स्तर पर किसी वस्तु का उठाने का भाव मन मे लाना भी चोरी मे आ जाता है।
4- ब्रह्मचर्य :- गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सामान्य जन जीवन मे ब्रह्म जैसा आचरण करना, अर्थात स्त्री पुरूष के मध्य नियन्त्रित रुप से भोग करना। उसमें लिप्त न होना ब्रह्मचर्य कहलाता है।
5- अपरिग्रह :- संग्रह न करना, अर्थात मनुष्य अपने जीवन मे उतना ही संग्रह करे जितनी आवश्यकता होती है।
~~~|~~|~~~~~~|~~~~|~~~~~|~~
2-नियम :- यह योग का दूसरा अंग है नियम ये भी पाँच हैं।
१-शौच :- शौच का अरथ है पवित्रता एवं स्वच्छता अपने शरीर को जल से स्वच्छ करना होता है। जल का सेवन करके शरीर के आन्तरिक यवयवो को स्वच्छ कर सकते है, सदाचार द्वारा आत्मा और मन को स्वच्छ रखकर बुरी भावनाओं का त्याग करके सह भावनाओं का ग्रहण कर आत्मा को स्वच्छ रखना शौच है।
२- संतोष :- इसमें जो मिल गया, उसी मे संतोष बनाये रखना, जब हमारे अंदर असंतोष पैदा करते है तो मनुष्य मे हिंसा, द्वेष, चोरी आदि दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं अतः हमें अपने जीवन मे संतोष रखकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए।
३- तप :- तप का अर्थ है सहनशीलता पैदा करना जन जीवन मे तप का गुफाओं मे जाकर समाधि लगाना नहीं वरन अपने अंदर शरीर एवं मन के स्तर पर सहन शक्ति पैदा करना, अपनी इन्द्रियों को वश मे रखकर सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि मे अनुकूल बनाए रखना।अर्थात प्रत्येक परिस्थितियों में ढाकना वास्तविक रु से तप कहलाता है।
४- स्वाध्याय:- अध्ययन द्वारा ज्ञान को बढ़ाना होता है, आज का युग वैज्ञानिक युग है, ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिकों ने राकेट का अविष्कार किया है।अपने गुण और अवगुण के बारे मे निरीक्षण करना उसके प्रति गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करना अपने अन्दर आत्म अवलोकन के भाव पैदा करना, सदग्रन्थों का अध्ययन करके उसके गुणों को ग्रहण करना वास्तविक स्वाध्याय है।
५- ईश्वर प्राणिधान :- इसका अर्थ है समर्पण किया जाय वह ईश्वर की आज्ञा समझकर किया जाए,ईश्वर की आज्ञा से संसार में धन वैभव का उपयोग किया जा सकता है। माता पिता, गुरुजनों के प्रति समर्पित भाव रखना, निर्धनों और दीन दुखियों की सेवा ईश्वर के अधीन है। अर्थात सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय- पराजय आदि ईश्वर के अधीन है।
3-आसन:-
∆∆∆∆ππ∆∆∆∆
मुख्यतः चार किये ही जाय।
अ- सिंहासन
ब- पदमा सन
स- सिद्धासन
द- भद्रासन
4- प्राणायाम:- प्राणायाम को जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्राणायाम के विषय मे कहा गया है कि जिस प्रकार अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर आ जाता है, उसी प्रकार श्वास को बल से बाहर फेंककर बाहर ही रोक देंऔर जब बाहर निकालना चाहे तो मूल इन्द्रियों को उस समय तक बाहर खींचे रखें जिसमें से श्वास बाहर निकालता है।इस प्रकार प्राण कि अधिक समय बाहर ठहर सकता है, जब घबराहट हो तो धीरे धीरे वायु को लेकर फिर भी वैसा करता चला जाये।
बाह्य– भीतर से निकली श्वास को बाहर ही रोक दे।
आभ्यान्तर– जब बाहर की साँस भीतर आए तो उसको अधिक से अधिक समय के लिए रोक दिया जाय।
श्वास– न प्राण बाहर निकले, न भीतर रहे अर्थात जहां का तहां।
बाह्यभ्यान्तर वृद्धि– जब साँस भीतर से बाहर की ओर आये तो रुक रुक आये।
अर्थात ” क्रमिक गति से साँस का आना और जाना प्राणायाम है, जिसमें नियमित गति से विराम आये ” ।
प्राणायाम १० प्रकार के मुख्य है।
1-पूरक कुम्भक रेचक
2- शीतली
3-सीतकारी
4- भ्रामरी
5- भस्त्रिका
6- उज्जायी
7- मूर्च्छा
8- सूर्य भेदी
9- चन्द्र भेदी
10- प्लावनी
5- प्रत्याहार :- महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के वर्णन मे इन्द्रियों के विषय से विमुख होने को प्रत्याहार माना है।
” स्वविषया सम्प्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार इवेन्द्रयाणां प्रत्याहारः ” ।
अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर इन्द्रियों का चित्त के स्वरुप में तदाकार हो जाना ही प्रत्याहार है।
इसमें इन्द्रयाँ बाह्य विषयों से विमुख होकर, विरक्त हुए चित्त के अनुरूप कार्य करने लगती हैं।
6- धारणा :- ” वृत्ति मात्र से चित्त को किसी एक देश मे स्थिर करना धारणा है ” ।
7- ध्यान :-
^^^^^^^^^^^^
महर्षि पतंजलि के अनुसार ” तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् “।
अर्थात जहां चित्त को ठहराया जाय वहीं वृत्ति का एक जैसा रहना ध्यान है।
अर्थात चित्तवृत्ति का ध्येय मे नितांत निमग्न हो जाना ही ध्यान है।
8- समाधि :-
#####$$$$#####
” तदेवार्थमात्र निर्भास स्वरुपशन्यमिव समाधि “
अर्थात जब ध्येय मात्र की ही प्रतीति होने लगे और चित्त का अपना स्वरुप शून्य हो जाय वहीं समाधि है ” ।
चित्त की उस वृत्ति को ध्यान कहते है जिससे ध्येय मे चित्त की तन्मयता हो जाय और ध्यान का अभ्यास करते करते जब चित्त ध्येय के आकार का हो जाय और अपने रुप का भी अभाव हो जाये, तब वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र ही भासित है, अन्य कुछ भी महसूस नहीं होता।
समाधि के दो भेद हैं:-
अ- सम्प्रज्ञान समाधि
ब- असम्प्रज्ञान समाधि
१- सम्प्रज्ञान समाधि :- इस समाधि में संसार का बीज विषय ध्येयाकार वृत्ति के रुप मे विद्यमान रहता है इसलिए इसे सबीज समाधि भी कहते है।
२- असम्प्रज्ञान समाधि :- इस समाधि मे ध्येयाकार वृत्ति भी शेष नहीं रहती इसलिए यह निर्बीज समाधि है।
समाधि मे विध्न ― आलस्य, प्रमाद,संशय,व्यथा,अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन,दौर्मनस्कता,लोलुपता और दुःख, भोगों की लालसा, विक्षेप,पसीना बहुत से विध्न आते हैं।
विशेष :- सभी सिद्धियां भी विघ्न रुप ही सिद्ध होती हैं।
” यदितन्नोपेक्षास्यात तदा मोक्षाद् भ्रष्टः कथं कृत कृत्यताभियात् ” ।
अर्थात इन सिद्धियों के चक्कर में योगी मोक्षमार्ग से भ्रष्ट हो जाते है।
महर्षि पतंजलि के अनुसार:-
” ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः “
ये सिद्धियां समाधि मे विघ्न स्वरुप है, पर जाग्रत अवस्था में आठ सिद्धियां है।
अतः स्वतः प्राप्त हो गई सिद्धियों का लाभ न उठावें, और इनके प्रदर्शन द्वारा किसी को चमत्कृत न करें।इन सिद्धियाँ मे वैराग्य होगा तो कैवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति होतीं है।